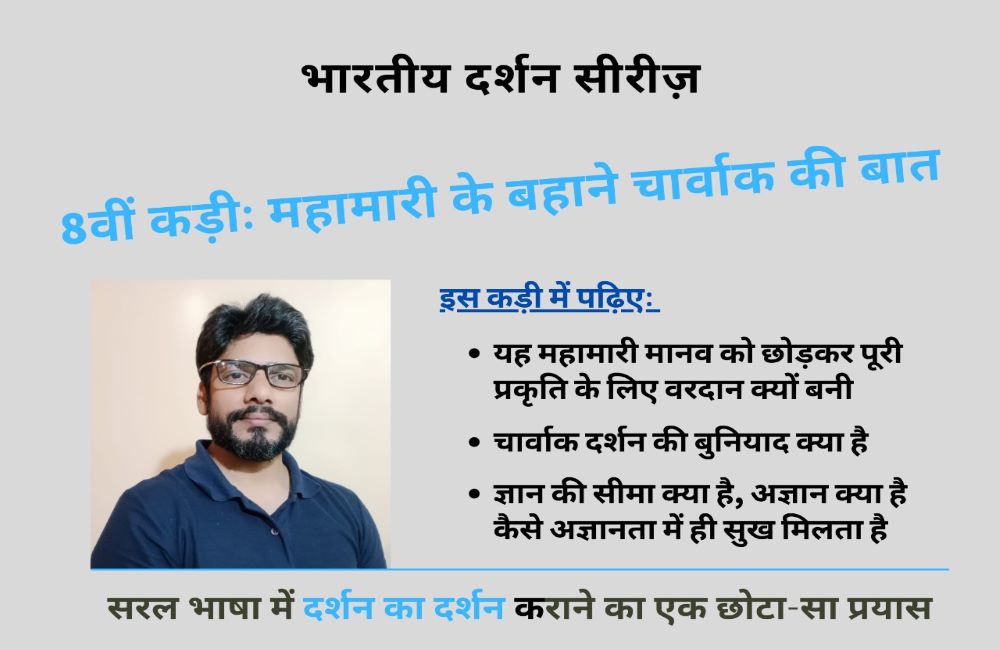अनुज राज पाठक, दिल्ली से, 27/4/2021
अभी 22 अप्रैल को ‘पृथ्वी दिवस’ था। यह पहला अवसर है, जब पूरी दुनिया के ‘मानव’ एक ही समय में एक जैसी महामारी से पीड़ित है। और इससे बड़े आश्चर्य की बात है कि यह महामारी मानव को छोड़कर अन्य समस्त प्राणियों, समस्त प्रकृति के लिए वरदान बनकर आई है।
विचारणीय यह है कि ऐसा क्यों? आज मानव के लिए सब संसाधन हैं। दोहन के स्रोत हैं। मानव यह नहीं सोचता कि हमारे जैसे अन्य प्राणियों के लिए, यहाँ तक कि स्वयं प्रकृति के लिए भी पृथ्वी जीवन का स्रोत है। दरअसल, इसी तरह तो स्वयं को केंद्र में रखकर आचार्य चार्वाक ने भी अपने दर्शन की नींव रखते हैं। प्राचीन काल में आचार्य चार्वाक की इसके लिए घोर आलोचना हुई थी। अतः उनका मत सीमाओं में सिमट कर रह गया। लेकिन आज क्या जाने-अनजाने हम सभी चार्वाक के अनुयायी नहीं हैं? हमारे लिए हम, हमारे शरीर का सुख ही सबसे अधिक महत्त्व नहीं रखता आज?
प्राचीन ऋषियों ने घोष किया यह पृथ्वी हमारी माता है (माता भूमि पुत्रोsहम् पृथिव्या:) । वह माता से अन्न जीवनयापन के लिए माँगता है। ज़बर्दस्ती माता से खींचता नहीं है। यह पृथ्वी भी मानव का पुत्रवत पालन करती रही। लेकिन आज हम केवल इस पृथ्वी को एक संसाधन मानकर उसका अनन्त दोहन करने लगे हैं। यही आचार्य चार्वाक का सिद्धान्त भी तो है। जी भरकर सुख लो। वह सुख किसे मानते हैं, “अङ्गनालिङ्गनाज्जन्य सुखमेव” (सर्वदर्शनसंग्रह)। अर्थात स्त्री आदि के आलिंगन से उत्पन्न सुख ही पुरुषार्थ है। और देह अर्थात शरीर का नष्ट होना मुक्ति है— “देहस्य नाशो मुक्ति:” (सर्वदर्शनसंग्रह)।
आचार्य वात्स्यायन भी अपने कामसूत्र में लोकायत मत के प्रसङ्ग में कहते हैं, ‘धर्म का आचरण ही न करें। क्योंकि इसका कोई फल नहीं है।’ (ना धर्माश्चरेत् का.सूत्र.1/2/25) । उसका समस्त केन्द्र शरीर है। वह उस शरीर को छोड़कर कुछ अन्य के विषय में विचार ही नहीं कर पाता। वह केवल भौतिक स्तर पर जीवन निर्वाह करता है वह भौतिक संसाधनों को एकत्र करने उनका भोग करने में लगा रहता है। अतः वह सीमित क्षेत्र उसके ज्ञान की सीमा है। जहाँ तक भूत दिखाई देते हैं, वही परिधि है। वह सीमितता अज्ञान है। वह उस अज्ञानता को ही सुख मानकर प्रसन्न रहता है।
जैसे एक गुबरैला (एक कीड़ा जो सदा ही गोबर का टुकड़ा मुँह में दबाए रहता है) जीवनभर गोबर में रहता है। उसका जन्म, जीवन और मरण के केन्द्र में गोबर रहता है। वह उसे ही प्राणों का आधार मानता है। उससे इतर देखना उसके लिए असम्भव है। समस्त प्रकृति का उसके लिए कोई महत्त्व नहीं। वैसे ही केवल भौतिक स्तर पर जीने वाले कि स्थिति होती है। उसके केन्द्र पदार्थ रहते हैं। पदार्थों की एक सीमा है। वह उस सीमा में बँध जाता है। वह शरीर और इन्द्रियों के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं मानता।
और अंततः अज्ञान में डूबकर स्वयं और सीमित ज्ञान से युक्त हो भौतिक पदार्थों के दोहन में लगा रहता है। सीमित सुख का भोग कर पाता है। इसके परिणामस्वरूप प्रकृति नष्ट होने लगती है। तो फिर वह कहीं ना कहीं सन्तुलन स्थापित करती है। इससे मानव विविध दैविक, भौतिक आपदाओं से त्रस्त हो त्राहिमाम कर उठता है।
कोरोना जैसी यह वैश्विक महामारी भी हमें इसी ‘दर्शन’ से साक्षात् करा रही है।
———
(अनुज, मूल रूप से बरेली, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दिल्ली में रहते हैं और अध्यापन कार्य से जुड़े हैं। वे #अपनीडिजिटलडायरी के संस्थापक सदस्यों में से हैं। यह लेख, उनकी ‘भारतीय दर्शन’ श्रृंखला की आठवीं कड़ी है।)