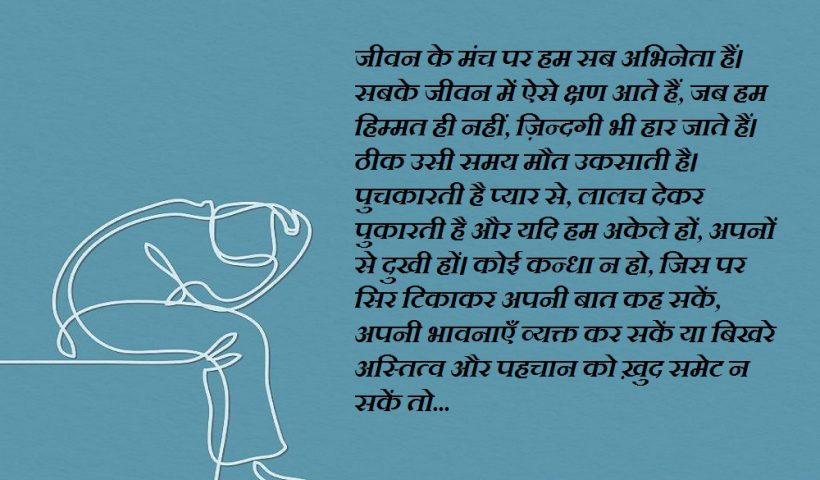हम सब स्तब्ध हैं। निशब्द हैं। दिमाग़ पंगु हो गया है। यदि कोई इस समय ज़रूरी मुद्दे या काम की बात कर ज्ञान-विज्ञान, समाज, संस्कृति,…
View More महामारी सिर्फ वह नहीं जो दिखाई दे रही है!Category: चुनिन्दा पन्ने
भारत की मुक्ति के लिए आज क्यों गाँधी जी के उद्धार की ज़रूरत है?
गाँधी जी भारत की तरह चिरन्तन हैं। वे भारत की महानता, बल, कमजोरी, सीमाएँ और सम्भावनाओं के प्रतीक हैं। जयन्ती के बहाने एक बार फिर…
View More भारत की मुक्ति के लिए आज क्यों गाँधी जी के उद्धार की ज़रूरत है?अफ़सर रिश्वत ले रहे, कोई बात नहीं; पर पकड़ में क्यों आ रहे?
वैसे तो ऐसे नाक़ारा देशभर में मिल जाएँगे, लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश में ये कुछ ज़्यादा ही पाए जा रहे हैं। अख़बार आए दिन…
View More अफ़सर रिश्वत ले रहे, कोई बात नहीं; पर पकड़ में क्यों आ रहे?कानून के लम्बे हाथों की दुहाई मत दो यार…ये हमने ठाकुर को लौटा दिए हैं…!
बीते दिनों मध्य प्रदेश के एक शहर में 800 से भी अधिक पुलिसकर्मियों ने मार्चपास्ट किया। मक़सद अपराधियों में ख़ौफ़ पैदा करना था। इससे अपराधियों…
View More कानून के लम्बे हाथों की दुहाई मत दो यार…ये हमने ठाकुर को लौटा दिए हैं…!बुद्ध कुछ प्रश्नों पर मौन हो जाते हैं, मुस्कुरा उठते हैं, क्यों?
एक बार बुद्ध के पास मौलुंकपुत्त नामक व्यक्ति आया। उसने बुद्ध से पूछा कि क्या वाक़ई ईश्वर है? बुद्ध ने ज़वाब दिया, “क्या वाक़ई में…
View More बुद्ध कुछ प्रश्नों पर मौन हो जाते हैं, मुस्कुरा उठते हैं, क्यों?महात्मा बुद्ध आत्मा को क्यों नकार देते हैं?
किन्हीं सेठ जी को अपने धन पर बहुत गर्व था। वे जब किसी को धन से मदद करते, तो सब जगह उसका बख़ान किया करते…
View More महात्मा बुद्ध आत्मा को क्यों नकार देते हैं?अधूरापन जीवन है और पूर्णता एक कल्पना!
हम सब अधूरे हैं। आधे-अधूरे काम करते हैं। अधूरेपन में जीते हैं। अधूरे रहकर ही जीवन समाप्त करते हैं। अपने अधूरेपन के कारण ही जीवन…
View More अधूरापन जीवन है और पूर्णता एक कल्पना!कृष्ण और बुद्ध के बीच मौलिक अन्तर क्या हैं?
श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर कृष्ण के विविध रूपों की लोगों ने अपने-अपने मतानुसार आराधना की। प्राय: श्रीक़ष्ण का बाल रूप और उनके उस स्वरूप की लीलाएँ हर व्यक्ति…
View More कृष्ण और बुद्ध के बीच मौलिक अन्तर क्या हैं?हम जितने वाचाल, बहिर्मुखी होते हैं, अन्दर से उतने एकाकी, दुखी भी
जीवन में जब होने, खोने और पाने के मायने जल्दी समझ आ जाते हैं, तो समझदार व्यक्ति ही आगे जाने या ख़ुद को ख़त्म करने…
View More हम जितने वाचाल, बहिर्मुखी होते हैं, अन्दर से उतने एकाकी, दुखी भीबुद्ध की बताई ‘सम्यक समाधि’, ‘गुरुओं’ की तरह, अर्जुन के जैसी
आतंक के शिकंजे में दबोचे जा चुके अफ़ग़ानिस्तान से आज, 24 अगस्त 2021 को गुरु ग्रन्थ साहिब की तीन प्रतियाँ भारत आई हैं। गुरु ग्रन्थ…
View More बुद्ध की बताई ‘सम्यक समाधि’, ‘गुरुओं’ की तरह, अर्जुन के जैसी